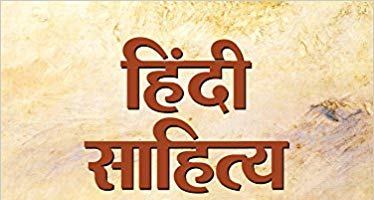
विश्व प्रसिद्ध इतालवी कवि दांते ने अपनी प्रसिद्ध कृति ‘‘ दि डिवाइ कामेडी ’’ में एक स्थान पर लिखा है : नरक में सबसे गर्म स्थान उन लोगों के लिए आरक्षित किया गया है जो नैतिक संकट के समय में या तो तटस्थ रहते हैं या बनने का प्रयास करते हैं। ’’
मुझे लगता है कि महान कवि दांते का यह कथन आज भी उतना ही परासंगिक है जो कि आज से कई शताब्दी पहले था। आज भी हमारे लेखक और कवि यह सोच कर अपनी रचनाएं सामने लाते हैं कि पता नहीं किस वर्ग को हमारी बात अच्छी लगेगी या बुरी। मैं सभों के बारे में तो यह नहीं कहता। मगर देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए तो ऐसा जरूर लगता है। हालांकि यह भी सच है कि अगर शिद्दत और पूरी तटस्थता से अगर कोई वर्ग अल्पसंख्यकों की समस्याओं को उठाता है तो वह हमारा बुद्धिजीवी यानि रचनाकार वर्ग और पत्रकार ही है।
इस विशेष वाक्य ने मुझे इस विषय पर लाने में भी एक प्रकार से प्रोत्साहित करने का काम किया। हम सब जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और ऐसा हम वर्षों से कहते, पढ़ते और सुनते हुए चले आ रहे हैं। जैसा समाज होगा, उसी प्रकार की रचनाएं हमारे सामने आएंगी। लेखक का स्तर भी उसका समाज ही निर्धारित करता है और उसकी रचनाओं को दिशा भी वही प्रदान करता है।
मुझे लगता है कि जब हम व्यापक रूप से साहित्य की भूमिका पर विचार करते हैं तो हमें साहित्य को किसी भी प्रकार की दर्जाबंदी में बांधने से बचना चाहिए। साहित्यकार का तो काम ही है उन सभी विषयों पर लिखना जो उसको उद्वेलित और परेशान करे। यदि कोई समस्या या घटना उसे परेशान नहीं करती, उसे खिन्न नहीं करती, उसे उदास नहीं करती, उसे उकसाती नहीं, उसे तंग नहीं करती, तो समझ लीजिए कि उस घटना या समस्या में बेहतर एवं प्रभावी साहित्य के रूप में अवतरित होने की संभावना न के बराबर है।
अब प्रश्न यह उठता है कि आजकल और विशेष रूप से भारत में वह कौन सी समस्याएं हैं जो किसी लेखक या कवि को कुछ लिखने के लिए अधिक प्रेरित कर रही हैं। अगर हम इस बिंदु पर विचार करें तो मुख्यतः कुछ विषय अधिक हमारे मन मस्तिष्क पर हावी होते दिखाई देते हैं। यदि 1947 के बाद की रचनाओं पर विचार करें तो हमारी समस्याएं कुछ और ही रूप में सामने आती हैं और अगर हम 1947 से पहले के समय पर विचार करते हैं तो हमारी समस्यओं का स्वरूप कुछ और ही था। 1857 के आस पास भारतीय समाज जिस परेशानी से गुजर रहा था उसका अद्भुत चित्रण उस काल के कवियों और लेखकों की कृतियों में देखने को मिलता है। उस वक्त मूल रूप से जो समस्याएं हमारे साहित्य के केंद्र में थीं वह अंग्रेजों की गुलामी से
उपजी समस्याएं थीं जैसे कि अस्मिता का प्रश्न, गुलामी का दर्द, गरीबी और भूख की चुभन, स्त्रियों एवं पिछड़े वर्ग की दयनीय स्थिति इत्यादि। उस समय सौभाग्य से सांप्रदायिकता एवं आतंकवाद हमारे साहित्य के विषय नहीं थे जो बीसवीं शताब्दी के अंत और इक्कीसवीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण विषय बन कर सामने आए हैं।
आखिर क्या वजह है कि भारत के दुखद विभाजन के बाद यह दोनों विषय केंद्र में आ गए, विशेष रूप से जब हम अल्पसंख्यक विमर्श की बात करते हैं। इसके अनेक कारण हैं और इसके लिए हमारे देश की राजनीति अधिक जिम्मेदार है जो यह मान कर चलती है कि इस देश पर अगर राज करना है तो यहां की जनता को केवल दो प्रकार से अधिक रूप से बेवकूफ बनाया जा सकता है और उसे अपनी जाल में फंसाया जा सकता है। वह है सांप्रदायिकता और आतंकवाद की आग में अनवरत झोंके रख कर। मुसलमानों से अब तो कदम कदम पर यह पूछा जाता है कि क्या आप सचमुच देश प्रेमी भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मुसलमान के रूप में आपकी भक्ति अरब देशों या फिर पाकिस्तान से है। यह भी दिलचस्प बात है कि जब मुसलमानों की
देशभक्ति पर संदेह किया जाता है और उसे देश निकाला देने की बात की जाती है तो पाकिस्तान के अलावह कोई और देश का नाम नहीं लिया जाता। न अरब देशों का न पड़ोसी देश बंगलादेश का जहां की बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है।
इससे यह पता चलता है कि मुस्लिम विरोधी भावनाएं पाकिस्तान तक जा कर सिमट जाती हैं क्योंकि यह देश हमारा पुराना शत्रु है और काशमीर पर हम से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष युद्ध भी वर्षों से लड़ता चला आ रहा है। भूख और गरीबी, बेरोजगारी, स्त्रियों की समाज में खराब हालत इत्याद विषय भी हमारे लेखकों को उद्वेलित एवं प्रेरित करते रहे हैं और मुस्लिम रचनाकार भी इन विषयों को उसी शिद्दत से उठाते रहे हैं जैसे कि अन्य धार्मिक वर्ग के हिंदी लेखक।
दिलचस्प बात यह है कि हिंदी के बेहद निकट मानी जाने वाली भाषा उर्दू एवं उसके साहित्य में इस प्रकार की दर्जाबंदी न तो की गई और अगर कभी करने का प्रयास भी किया गया तो उसे अधिक प्रोत्साहित नहीं किया गया। वहां फिराक गोरखपुरी, राम लाल, गोपी चंद नारंग, तरन नाथ शरशार, ब्रज नारायण चकबस्त, प्रेमचंद, कृष्ण चंद, राजेंद्र सिंह बेदी, गुलजार इत्यादि सारे बड़े लेखक उर्दू साहित्य का एक अटूट हिस्सा हैं और उन्हें केवल उर्दू रचनाकार के रूप में ही याद और सम्मानित किया जाता है। कोई यह नहीं कहता कि उर्दू के हिंदू लेखक।
एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं कि साहित्यिक विमर्श करते समय अगर हम खानाबंदी का शिकार हुए तो शायद हम इतने गंभीर विधा के साथ अधिक इंसाफ नहीं कर पाएंगे। उसके अनेक कारण है। सबसे पहले जो मुझे लगता हैकि लेखक तो लेखक होता है, वह लिखते वक्त न तो हिंदू होता है न मुसलमान, न सिख और न ईसाई या जैन। लेखक और कवि समाज को सबसे संजीदा व्यक्ति कहलाता है और उसकी संजीदगी और उसकी गंभीरता ही उसे इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बिना किसी का पक्ष लिए या विद्वेष रखे हुए अपनी बात बेबाकी और सफाई के साथ रखे। उसके लिए चाहे वह जो भी साधन अख्तियार करे। वह कविता हो सकती है, उपन्यास हो सकता है या कहानी हो सकती है या लेख हो सकता है। इसको एक उदाहरण के रूप में यहां स्पष्ट करना चाहूंगा।
मेरा संबंध ऐतिहासिक भूमि चंपारण, बिहार से है जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने सत्याग्रह का आरंभ किया था। उस जिले में जिस थाना और क्षेत्र से मेरा संबंध है, वह मुस्लिम बहुल है। और विशेष रूप से मेरा गांव तो सत प्रतिशत मुस्लिम बहुल गांव है। लगभग बीस हजार की आबादी वाले इस गांव में केवल दो तीन दर्जन लोग ही बहुसंख्यक समाज से आते हैं। उनमें भी वे सारे लोग दलित समाज के हैं जिन्हें वैसे भी भारतीय समाज में आज भी दुभार्ग्य से वह मकाम हासिल नहीं हुआ जिसके वे हकदार हैं।
एक लंबे समय तक मैं इस एहसास के तेहत जीता रहा है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदू किस प्रकार अल्पसंख्यक के रूप में जिंदगी गुजारते हैं। उनकी समस्याएं क्या हैं। उनकी सोच और उम्मीदें क्या हैं। तो मैं ने पाया कि उनकी सोच और हमारी सोच में एक इंसान के रूप में कोई फर्क नहीं था। एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पत्नी के रूप में , एक बहन के रूप में सब एक जैसे हैं। उन लोगों के परिवार के साथ मेरे परिवार का भी बहुत घनिष्ठ संबंध था। हर माले में सब प्यार मुहब्बत से और मिल जुल कर रहते थे। एक दूसरे के तीज त्योहार में शरीक होते थे। यह प्रेम और सौहार्द की स्थिति उस समय तक बनी रही जब मंदिर मस्जिद के झगड़े ने देश को अपनी चपेट में नहीं ले लिया। बाबरी मस्जिद का ढ़ांचे गिरने के बाद जिस प्रकार देश में सांप्रदायिक उन्माद फैला उसका शिकार मेरा गांव और वहां अल्पसंख्यक रूप से रहने वाले हिंदू भाई भी हुए। यकायक उनमें अपनी असुरक्षा का भाव गहराने लगा और वे मुस्लिम बहुल गांव से पलायन करने के बारे में सोचने लगे। और उसमें वह कामयाब भी हुए। भले ही जहां वह बहुत उम्मीदें ले कर गए वहां जाति के आधार पर स्वयं उनके अपने हिंदू भाईयों ने उन्हें बहुत प्रताड़ित और अपमानित किया। ठीक वैसा ही जैसा कि देश विभाजन के बाद भारत से गए मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के मूल निवासियों ने किया।
लेकिन इस घटना का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ। और मैं ने इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक सोचना शुरू कर दिया। जिसका नतीजा एक उपन्यास की शक्ल में सामने आया जिसका नाम था, ‘‘जो अमां मिली तो कहां मिली’’। और सौभाग्य से इसे संस्कृति पुरस्कार से नवाजा गया। यहां इस उदाहरण के माध्यम से जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि लेखक किसी घटना या समस्या को धर्म या जाति की निगाह से नहीं देखता। वह तो समस्या को इंसानी बुनियाद पर देखता और परखता है। और अगर वह ऐसा न कर पाए तो फिर वह अच्छी रचना सामने ला ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं इस प्रकार की साहित्कि दर्जाबंदी को सिरे से नकारता हूं। लेकिन चूंकि आज के हिंदी साहित्य विमर्श में अल्पसंख्य विमर्श को प्रचलित शब्दावली के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, इस दृष्टि से भी कुछ बातें यहां करना आवश्यक जान पड़ता है।
हिंदी में वैसे तो अल्पसंख्यक विमर्श का अर्थ उस साहित्य से लिया जाता है या जा रहा है जिस साहित्य को मुस्लिम हिंदी लेखकों ने स्वयं अपने समाज के बारे में लिखा हो। और उनमें जो नाम प्रमुख रूप से सामने आते हैं उनमें शानी, राही मासूम रजा, असगर वजाहत, अब्दुल बिस्मिल्लाह, मंजूर एहतेशाम इत्यादि कुछ बेहद ही प्रतिष्ठित नाम हैं। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यह सूची अधिक लंबी नहीं है और इन ही चंद गिने चुने लेखकों तक आते आते सिमट सी जाती है। इक्कीसवीं शताब्दी को गुजरे अभी केवल साढ़े सत्तरह वर्ष ही हुए हैं और इसमें कोई अन्य दूसरा प्रतिष्ठित मुस्लिम लेखक या कवि इन नामों के अलावह नजर भी नहीं आ रहा। हालांकि सैकड़ों मुस्लिम रचनाकार हैं जो हिंदी साहित्यिक जगत में अपना नाम स्थापित करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मगर यह आने वाला समय ही बताएगा कि उनमें कितने कामयाब हो पाते हैं और कितने नाकाम होते हैं।
प्रसिद्ध मस्लिम कवियों और लेखकों की रचनाओं पर यदि बारीकी से नजर डालें तो ऐसा लगता है कि उनके लेखन में वही दर्द और छटपटाहट है जो अन्य धर्म या जाति से आने वाले रचनाकारों के यहां मौजूद है। सभी ने अपने अपने समाज की समस्याओं, उसकी विसंगतियों पर पर्दा उठाने की कोशिश की है। किसी का संबंध जागीरदाराना समाज से है तो उसने अपने समाज की उन ही समस्याओं पर कलम उठाया है। किसी का संबंध निम्न वर्ग से है तो उसने उस पर लिखा है। मगर उन पात्रों के नाम यदि हटा दिए जाएं और उसे कोई तटस्थ सा नाम दे दिया जाए तो फिर यह फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि यह समस्याएं हिंदू समाज की हैं या मुस्लिम समाज की हैं।
हिंदू और मुसलमान इस देश में सदियों से एक साथ रहते आए हैं और अधिकांश मुसलमानों का तअल्लुक इसी धरती से रहा है और है। उनके बाप दादा यहीं पैदा हुए और यहीं मरे। उनकी भाषा एवं संस्कृति भी एक जैसी है। जो चीज उनमें फर्क करती है वह भी केवल किसी हद तक, वह है उनकी धार्मिक पहचान और रीति रिवाज और खान पान एवं पहनावा। बाकी संवेदनाएं एक, सोच एक, समस्याएं एक। गरीबी और बेरोजगारी ही बुनियादी तौर पर उन्हें परेशान करती दिखाई देती हैं। स्त्रियों एवं दलितों का शोषण तो प्रत्येक वर्ग के रचनाकारों को परेशान करता रहा है। चाहे वह प्रेमचंद हों, कमलेश्वर हों, उपेंद्रनाथ अश्क हों या अन्य प्रसिद्ध लेखक एवं कवि हों, उन सभों ने मुस्लिम समाज और उनके भीतर की समस्याओं पर भी बड़ी बारीकी से कलम उठाया है।
प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों पर अपनी बात समाप्त करता हूंः अल्पसंख्यकों के आँसू यदि पुछे नहींए
वृथा देश में तो कायम सरकार है। बहुमत को तो अलम स्वयं अपना बल हैए अल्पसंख्यकों का शासन पर भार है।
लेखक : डा. मोहम्मद अलीम


